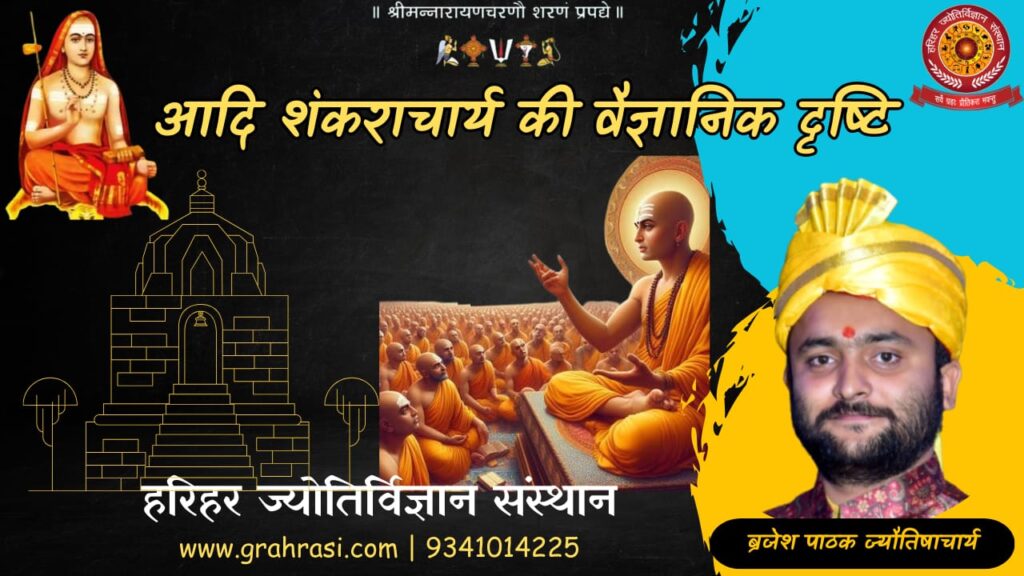
आदि शंकराचार्य जी का परिचय –
शिवावतार आदि-शंकराचार्य महाभाग का नाम तो आप सब जानते ही हैं, उनके ही द्वारा अनेकों ग्रंथों एवं स्तोत्रों की रचना की गई है। सर्वप्रथम मैं आदि-शंकराचार्य महाभाग का सुसंक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आद्य-शंकराचार्य के जन्म को लेकर मतैक्य नहीं है।
गोवर्धनपीठ पुरी के परंपराप्राप्त शंकराचार्य परमादरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी रूपी आप्तप्रमाण के अनुसार आदि-शंकराचार्य जी का जन्म युधिष्ठिर संवत् 2631 तदनुसार 507 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल पञ्चमी को हुआ था।1
विकिपीडिया के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508-9 ईसा पूर्व में तथा निर्वाण 477 ईसा पूर्व में हुआ था।2 हाँलाकि नीचे इसी लेख के अन्तर्गत लिखित ‘जीवनचरित‘ अनुभाग में विकिपीडिया ने आदि-शंकराचार्य जी का जन्म 507 ईसा पूर्व लिखा है।
सन् 1949 में आदि-शंकराचार्य विरचित सौन्दर्य लहरी पर स्वामी विष्णुतीर्थ जी की टीका प्रकाशित हुई थी। इसकी PDF इन्टरनेट पर उपलब्ध है।3 उसके प्रारम्भ में ही विनायकराव बापूजी वैशम्पायन द्वारा लिखित “श्रीमच्छंकर भगवत्पाद की जीवन झांकी और सौन्दर्य लहरी” नामक लेख प्रकाशित है, इसमें विनायकराव जी ने डॉ. भाण्डारकर, जस्टिस तैलंग, लो. तिलक आदि अनेकों विद्वानों का हवाला देते हुए 788 ई. में आदि-शंकराचार्य जी का जन्म लिखा है।
आदिशंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालपी (कालडी या काषल) ग्राम में हुआ था। इनके दादा का नाम विद्याधिराज, पिता का नाम शिवगुरु भट्ट तथा माता का नाम सुभद्रा (आर्याम्बा) था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव की आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्र-रत्न पाया था, अत: उसका नाम शंकर रखा। जब ये तीन ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया।
ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। छह वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और आठ वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनके गुरु का नाम गोविन्दपाद था। आदि शंकराचार्य जी का मण्डन मिश्र और उनकी पत्नी भारती के साथ शास्त्रार्थ तथा परकाया प्रवेश की कथा सुप्रसिद्ध है।

- 1 भगवत्पाद शिवावतार भगवान् शंकराचार्य महभाग का 2527वां प्राकट्य महोत्सव – YouTube
2 आदि शंकराचार्य – विकिपीडिया (wikipedia.org)
3 सौंदर्य लहरी हिन्दी पुस्तक | Saundarya Lahari Hindi Book PDF (hindihearts.in)
इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। धर्मरक्षा के लिए आदि-शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन संन्यासी ‘शंकराचार्य’ कहे जाते हैं।
वे चारों स्थान ये हैं-
- (१) ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम
(२) श्रृंगेरी पीठ
(३) द्वारिका शारदा पीठ और
(४) पुरी गोवर्धन पीठ।
इसलिए परंपराप्राप्त मान्य शंकराचार्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती, फिर भी बहुत खेद और दुर्भाग्य की बात है, आजकल भारतवर्ष में कलिप्रभाव से छद्म शंकराचार्यों की भरमार हुई पडी है।
आदि-शंकराचार्य ने अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त की स्थापना की तथा उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधानकारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान-कर्मसमुच्चयवाद का खण्डन किया। आदि-शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी (श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखा जो बहुत प्रसिद्ध है।
इसके अलावा उन्होंने विवेकचूड़ामणि आदि अनेकों स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना की और अनेकों स्तोत्र आदि भी रचे। आदि-शंकराचार्य जी के साहित्य की तीन शैली है। एक तो भाष्य (जैसे श्रीमद्भगवद्गीता और विभिन्न उपनिषदों पर किया गया भाष्य), दूसरा प्रकरण ग्रन्थ (जैसे विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, अपरोक्षानुभूति आदि), तीसरा स्वतन्त्र स्तोत्र आदि।
उन्होंने बहुत से स्तोत्र जैसे शिव मानसपूजा, कृष्णाष्टकम्, भवान्यष्टकम्, कालभैरवाष्टकम्, निर्वाणषट्कम् आदि लिखे हैं। भारतवर्ष में धर्म की पुनर्स्थापना करने के पश्चात् ३२ वर्ष की अल्पायु में ही आदि-शंकराचार्य जी ने केदारनाथ के समीप अपनी लीला का संवरण करते हुए शिवलोक प्रयाण किया।1
आदि शंकराचार्य जी के ग्रन्थों में आधुनिक विज्ञान के अन्तर्गत अतीन्द्रिय शक्ति, मनोविज्ञान, भोजन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सृष्टि विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा प्राप्त होती है।
आदि शंकराचार्य जी की वैज्ञानिक दृष्टि को यदि समझना हो तो विशेषकर उनके द्वारा लिखित श्रीमद्भगवद्गीता के सप्तम, अष्टम, त्रयोदश, पञ्चदश और अष्टादश अध्यायों के शांकर भाष्य को देखना चाहिए साथ ही अपरोक्षानुभूति में भी उन्होंने बहुत ही अद्भुत सिद्धान्त प्रदान किए हैं।
1 षट्पदीस्तोत्रम्, कमला टीका, डॉ. विन्ध्येश्वर पाण्डेय, Notion Press, Chennai, 2022
आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन के एक प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। उनके विचार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सार्थक हैं। इस शोधलेख में, हम शंकराचार्य की वैज्ञानिकी दृष्टि के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।
1. अद्वैत वेदांत की वैज्ञानिकी दृष्टि : ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या
अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया है। इस सिद्धांत के पीछे गहरी वैज्ञानिक दृष्टि है। ब्रह्मज्ञानावली मालिका में आदि शंकराचार्य ने कहा है –
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥1
अर्थात् – ब्रह्म वास्तविक है, ब्रह्मांड मिथ्या (आभासी) है। जीव ही ब्रह्म है, यह ब्रह्म से भिन्न नहीं। इसे सही शास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस सृष्टि को समझते तथा महसूस करते हैं, वह सब वास्तविकता से दूर है, आभासी है या भ्रम है अर्थात् माया है। यह माया एक तरह की मृगतृष्णा या मरुमरीचिका है।
अगर हम गर्मी के समय में मार्ग में या खुले स्थान में या मरुभूमि में देखें तो कभी-कभी काफी दूरी पर हमें पानी सा कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पानी बिलकुल नहीं मिलता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ प्रकाश का कुछ ऐसा परावर्तन हुआ था, जिसने दूर से पानी होने का भ्रम पैदा कर दिया।

स्पष्ट है कि वहाँ कुछ था, जो दूसरे के होने का भ्रम पैदा कर रहा था। इसी प्रकार आप जिसे ‘मैं’ समझ रहे हैं, वास्तव में वह केवल ‘मैं’ नहीं बल्की सबकुछ है, यही माया है। आप जिसे (ब्रह्म को) दूसरा समझ रहे हैं, वह वास्तव में आप ही हैं। आप जिसे सबकुछ समझ रहे हैं, वह सबकुछ होते हुए शून्य भी है। आदि शंकराचार्य इसी माया की बात कर रहे हैं।
माया मायाकार्यं सर्वं महदादि देहपर्यन्तम्।
असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम् ॥2
आदि शङ्कराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रन्थ में कहा है कि सबकुछ ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। आदि शंकराचार्य जी के इस कथन से स्पष्ट है कि सृष्टि और उसका रचयिता एक ही है।
ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूतेऽथर्वनिष्ठा वरिष्ठा।3
- 1 https://sanskritdocuments.org/sites/snsastri/brahmajnaanaavalimaalaa.pdf
2 विवेक-चूडामणि श्लो.233, पृ.सं.64, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
3 विवेक-चूडामणि श्लो.125, पृ.सं.36, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
इसका गूढार्थ यह हुआ कि मानव सरल सुलभ स्वयं को जानकर उस जगत्नियन्ता ब्रह्म को जान सकता है। आधुनिक भौतिक शास्त्र भी आपसे यही तो कह रहा है कि पूरा ब्रम्हांड बुनियादी तौर पर एक ही ऊर्जा है। इस सन्दर्भ में आप बिग बैंग थ्योरी को पढ़ सकते हैं, विशेषकर Poe (Edgar Allan Poe) का विचार सुस्पष्ट, महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है।1
आज आदि शंकराचार्य जी के जन्म के हजारों वर्षों बाद अपनी शैली में अनकों शोध एवं प्रयोग करने बाद Cosmology के आधुनिक विज्ञान ने भी इन मतों को सिद्ध कर दिया है, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य जी और तमाम ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पूरी स्पष्टता के साथ कह दिया था।
1.1 ब्रह्म : अनंत ऊर्जा का स्रोत
ब्रह्म को अद्वैत वेदांत में अनंत और अपरिवर्तनीय माना गया है। आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रसिद्ध है इस सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।2 अब जरा आदि शंकराचार्य कृत अपरोक्षानुभूति नामक ग्रन्थ के इस श्लोक को देखिए –
ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः।
तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तित्यवधारयेत् ॥3
अर्थात् – सबकुछ परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अतः सबकुछ ब्रह्म ही हैं ऐसा समझना चाहिए।
इससे सुस्पष्ट है कि ब्रह्म ऊर्जा ही हमें अलग अलग रुपों में देखने को मिलती है। आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित ब्रह्म का यह सिद्धांत और ऊर्जा का वैज्ञानिक सिद्धांत एक-दूसरे के पूरक हैं।
क्वांटम यांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटनों या आश्चर्यजनक खोजों में से एक है -Principle of Superposition4, जो यह मानता है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। इस घटना को डबल-स्लिट प्रयोग द्वारा प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया गया है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे कण दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं – तरंग जैसे गुण भी और कण जैसे गुण भी।
जब उनका अवलोकन नहीं किया जाता है, तो वे एक साथ कई पथों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे एक व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। हालाँकि, जब अवलोकन किया जाता है, तो कण एक ही अवस्था में सिमट जाते हैं, अलग-अलग कणों की तरह व्यवहार करते हैं।
उक्त बातों को समझ चुकने पर विवेक चूड़ामणि के प्रस्तुत श्लोक पर भली-भाँति गौर करें।
ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च।
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ।।
अर्थात् – सभी नाम विविध रूप और सम्पूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है ऐसा श्रुति (वेद) ने कहा है।
यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि एक ही ब्रह्मशक्ति एक ही समय पर अलग-अलग गुण प्रदर्शित कर सकती है अर्थात् अलग-अलग व्यवहार कर सकती है। इसलिए पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित अलग-अलग स्वरूपों में दिखने वाले ब्रह्म का गुण और व्यवहार भी अलग-अलग है। कदाचित् यह हो सकता है क्वांटम यांत्रिकी का Principle of Superposition आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित ब्रह्म के उक्त सिद्धांत से प्रेरित हो।
1.2 जगत : माया और यथार्थ
मा माने धातु से ‘माच्छाससिसूभ्यो यः’ इस उणादिकोशीय सूत्र से य प्रत्यय करने पर माय इस प्रकार स्थिति होने पर पुनः टाप् प्रत्यय से यह माया शब्द सिद्ध होता है। मीयते अपरोक्षवत् प्रदर्श्यतेऽनया इति माया, मीयते निर्मीयते जगत् यया सा माया, मीयते ज्ञायते आत्मनि अध्यस्तं जगत् यया सा माया इत्यादि प्रकारों से इसकी व्युत्पत्ति होती है।
अपरोक्ष रूप से जिसके द्वारा यह संसार मापा जाता है, जो इस संसार को मापती है तथा बनाती है और जिसके द्वारा आत्मा में इस जगत् का ज्ञान होता है वह माया कहलाती है। श्रुति तथा स्मृतियों में माया – अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, मिथ्याज्ञान, अव्यक्त, अव्याकृत, महासुषुप्ति तथा अक्षर इत्यादि शब्दों के द्वारा जानी जाती है।5
अद्वैतवेदान्त में जगत् के उपादान के स्वरूप में माया को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से माया श्रुति तथा स्मृति के द्वारा सिद्ध है। माया को समझना परम दुरूह बताया गया है।

- योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति6
( जो हमें अविद्या से पार तारती है ) - मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्7
( माया को प्रकृति समझना चाहिए तथा मायापति को महेश्वर ) - इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 8
( इन्द्र माया के द्वारा पुरुष रूप में देखा जाता है ) इत्यादि श्रुतियों में - मम माया दुरत्यया9
( मेरी माया को समझना कठिनतम है ) - नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः10
( योगरूप माया ढका हुआ होने के कारण में सभी का प्रकाश नहीं हूँ ) - अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव11
(अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है जिससे जन्तु मोहित हो जाते हैं )
इस प्रकार से शास्त्र के वचनों में माया के सत्त्व तथा माया युक्त ईश्वर का ही जगत् के कर्तृत्व रूप में वर्णन है। बद्धजीव माया से निर्मित इस प्रपञ्च में अन्तः करण देह इन्द्रियों के द्वारा एक का अनुभव करता हुआ स्वयं कर्ता तथा भोक्ता होता है और सुखदुःख का अनुभव करता है।
आदि शंकराचार्य जी के अनुसार, जगत एक माया है, जिसका अर्थ है कि यह अस्थायी और परिवर्तनीय है। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों जैसे कि क्वांटम यांत्रिकी और रिलेटिविटी से मेल खाता है। क्वांटम यांत्रिकी में, पदार्थ की मौलिक इकाइयां (क्वांटम) भी अस्थायी और अनिश्चित होती हैं। इसको समझने के लिए आप Heisenberg Uncertainty Principle, Principle of Superposition, Quantum Entanglement इत्यादि को पढ़ सकते हैं।12
2. पर्यावरण के प्रति जागरूकता
शंकराचार्य ने ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त माना, जिसका अर्थ है कि हर जीव और निर्जीव वस्तु में ब्रह्म का अंश है। शंकराचार्य के इस दृष्टिकोण से हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति का हर तत्व ब्रह्म का हिस्सा है, इस जगत में ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं है।13
आप स्वयं विचार करें, यह कितना उच्च विज्ञान है और कितनी उत्कृष्ट सत्यता है। यदि मानव इस सत्य को आत्मसात कर ले तो यह समस्त संसार समस्त सृष्टि सुखी हो जाएगी। कहीं पर्यावरण का दोहन नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रदुषण नहीं होगा, कहीं जीव हत्या नहीं दिखेगी, कोई जीव या मानव पीडित नहीं दिखेगा, कोई ग्लोबल वार्मिंग नही, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, कहीं हत्या, लूट-पाट या बलात्कार नहीं, सारे कोर्ट कचहरी, जेल खाली नजर आएँगे।
वाह… कितना सुन्दर संसार होगा। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रदान की गई केवल इस एक शिक्षा को यदि हम आत्मसात कर सके अपने बच्चों को इसे सिखा सके, इसे अपने संस्कार में ढाल सकें तो क्या समस्त विश्व में कहीं कोई समस्याएँ दिखाई देंगी ???
यह कितना बडा विज्ञान है जो स्वयं सभी अज्ञान को मिटाने की क्षमता रखता है। हम कोई भी अपराध अज्ञान में करते हैं अगर हमें इस विज्ञान का ज्ञान हो जाए समस्त अज्ञान का नाश हो जाएगा और समस्त अज्ञान के नाश होने से सभी अपराध भी मिट जाएँगे।
आधुनिक विज्ञान भी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जोर देता है, जो शंकराचार्य की शिक्षाओं के अनुरूप है। शंकराचार्य के विचारों में सभी जीवों की एकता का संदेश मिलता है। यह जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करता है, जो आज के वैज्ञानिक युग में अत्यंत प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण है।
3. तर्क और विवेक
3.1 तर्क की महत्ता
तर्क वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। विज्ञान में हर सिद्धांत को तर्क, प्रमाण, परीक्षण और अनुभव के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। आदि शंकराचार्य जी की कृतियों में आपको ये सभी सिद्धांत सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने सिद्धान्तों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त तर्क और उदाहरण दिए हैं। पाठकों के संज्ञान के लिए एक उल्लेखनीय तर्क प्रस्तुत है –
मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्
न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः॥14
अर्थात् – मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक् नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिकारूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक् नहीं है, अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाममात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है ?
प्रसंगवशात एक उल्लेखनीय उदाहरण भी प्रस्तुत है –
घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बमालोक्य मूढो रविमेव मन्यते।
तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥15
अर्थात् – जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिम्बित सूर्य बिम्ब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानीपुरुष भ्रम से अपना ‘आप’ ही मान बैठता है।
3.2 माया और मिथ्या का विवेक
जीव स्वरूप से तो ब्रह्म के समान ही होता है। माया के कारण ही उसका स्वरूप अपरोक्ष नहीं होता है। माया को समझने के लिए हम कई उदाहरण ले सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। माया का मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। माया का मतबल एक भ्रम है, एक आभास है। अर्थात् कोई चीज वास्तव में जैसी है, उसे आप वैसा नहीं देख रहे हैं।

उदाहरण के लिए आप अपने शरीर को ही ले लें। आप एक भौतिक शरीर के रूप दिखाई देते हैं, लेकिन जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं अथवा जो हवा आप सांस के रूप में लेते हैं, उनसे हर क्षण आपके शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन हो रहे हैं।
आपके ऊतक एवं शरीरांग कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों के भीतर पूरी तरह से बदल कर पुनर्जीवित हो जाते हैं। आपके शरीर में पुरानी कोशिकाओं का नष्ट होना और नवीन कोशिकाओं का बनना निरन्तर चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ समय बाद आप पूरी तरह से एक नया शरीर होते हैं। लेकिन अपने अनुभव में आपको ऐसा लगता है कि यह वही शरीर है, यही आभास माया है।
आदि शंकराचार्य ने जगत को मायाकार्य कहा, परंतु माया को पूरी तरह मिथ्या नहीं माना। उनका कहना था कि जगत का अनुभव (माया) यथार्थ है, परंतु इसका अंतिम सत्य ब्रह्म है।16
यह दृष्टिकोण विज्ञान में सापेक्षता के सिद्धांत के समान है, जहां वस्तु और समय, समय और स्थान तथा ऊर्जा और द्रव्यमान का अनुभव सापेक्ष होता है। इसके लिए आप Theory of Relativity के अन्तर्गत General Relativity और Special Relativity के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं।17
4. मनोविज्ञान और आत्मा का संबंध
आदि शंकराचार्य जी ने आत्मा और मन के संबंध पर विचार किया। उन्होंने विवेक चूड़ामणि के अनात्मनिरूपण प्रकरण में मन को अनात्म बताया है –
देहेन्द्रियप्राणमनोऽहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः।
व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वमव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा ॥18
अर्थात् – देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि सम्पूर्ण विषय, आकाशादि भूत और अव्यक्तपर्यन्त निखिल विश्व – ये सभी अनात्मा (आत्मा इनसे भिन्न है) हैं।

उन्होंने ‘आत्मबोध’ नामक ग्रन्थ में यह भी बताया है कि मनोमयादि कोश से आवृत्त होने के कारण आत्मा भी तत्तन्मय तुल्य दिखाई देता है। इससे मन और आत्मा के बीच गहरे सम्बन्ध की स्पष्ट प्रतीति होती है।
पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः।
शुद्धात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा॥19
अर्थात् – जैसे स्फटिक नीले पीले आदि वस्त्रों के संयोग से नीला पीला आदि रंगों से युक्त प्रतीत होता है वास्तव में स्फटिक स्वच्छ सफेद है इसी तरह आत्मा भी निर्मल और शुद्ध है, वह पंच कोशादि के योग से कोशरूप प्रतीत होता है। पंचकोश – अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोश, विज्ञानमयकोश, और आनन्दमयकोश। इन्हीं पांचों कोशों के योग से आत्मा भी तत्तन्मय कोशतुल्य दिखाई देता है।
मन और आत्मा के बीच का गहरा सम्बन्ध विवेक चूड़ामणि के आत्म-निरूपण प्रकरण में आदि शंकराचार्य जी की निम्नलिखित पंक्तियों से और भी स्पष्ट हो जाता है –
यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः।
विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव ॥20
अर्थात् – जिसकी (जिस आत्मा की) सन्निधि मात्र से देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित होकर अपने-अपने विषयों में बर्तते (प्रवृत्त होते) हैं।
यह सकल प्रपंच सद्-ब्रह्मकार्य है अतः ब्रह्म का ही अंश है।21 इसी प्रकार मनुष्य का मन और आत्मा एक ही ब्रह्म का अंश हैं। यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाता है, जहां मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का आपसी संबंध माना जाता है।
शंकराचार्य की आत्मानुभूति की अवधारणा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आत्मानुभूति के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के दुःखों से आत्यन्तिक मुक्ति पाकर मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है, जो आजकल चहुँओर व्याप्त मानसिक अस्वस्थता के निवारण में अत्यन्त सहायक है।
वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् ।
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥22
अर्थात् – वेदान्त वाक्यों के अर्थका विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार-दुःख का आत्यन्तिक नाश हो जाता है।
5. विज्ञान और अध्यात्म का मेल
आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के प्रमाणों से अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों को पुष्ट किया। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत को विस्तार से बताया गया है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकता है।
उपनिषदों में जीवन की मौलिक संरचना और ब्रह्म के सिद्धांत का वैज्ञानिक रीति से अद्भुत् आध्यात्मिक विश्लेषण मिलता है। शंकराचार्य की तार्किक दृष्टि ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी प्रेरणा प्रदान की है।
उनके विचारों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की मौलिक संरचना और जीवन के सिद्धांतों को समझने के लिए प्रेरित किया है। अनेकों वैज्ञानिकों ने आदि शंकराचार्य जी की कृतियों से प्रेरणा ली है।
निष्कर्ष
आदि शंकराचार्य की दृष्टि में न केवल आध्यात्मिकता थी, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को तार्किक दृष्टिकोण से देखा। उनकी विचारधारा में तर्क, विवेक, पर्यावरण जागरूकता, मनोविज्ञान और आत्मानुभूति का समावेश था, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भी सामंजस्य बैठाता है।
उनकी शिक्षाएं आज तो अत्यन्त प्रासंगिक हैं और उनके विचारों को समझने से हमें न केवल आध्यात्मिक, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ हो सकता है। शंकराचार्य की आध्यात्मिक और तार्किक दृष्टि हमें सिखाती है कि अध्यात्म न केवल विज्ञान का सहायक सिद्ध हो सकता है, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक तथा प्रेरक हो सकते हैं।
1 History of the Big Bang theory – Wikipedia
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy
3 अपरोक्षानुभूति (203), श्लो.49, पृ.सं.13, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत्
4 https://www.techtarget.com/whatis/definition/superposition
5 उच्चतर माध्यमिक भारतीय दर्शन, पाठ 12, पृ.सं.16, https://www.nios.ac.in/media/documents/bgp/347_Bharatiya_Darshan/Hindi_Medium/L12.pdf
6 प्रश्न-उपनिषद्, शांकरभाष्य, प्रथम-प्रश्न, श्लो.सं.8, रामकृष्णमठ, नागपुर 2023
7 श्वेताश्वतरोपनिषद्, शांकरभाष्य, अ.4 श्लो.10, पृ.सं.185, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 1995
8 बृहदारण्यकोपनिषद्, अ.2, ब्राह्मण 5, गद्य 19, पृ.सं.610, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2058
9 श्रीमद्भगवद्गीता (18) अ.7 श्लो.14, पृ.सं.102, गीताप्रेस गोरखपुर
10 श्रीमद्भगवद्गीता (18) अ.7 श्लो.25, पृ.सं.105, गीताप्रेस गोरखपुर
11 श्रीमद्भगवद्गीता (18) अ.5 श्लो.15, पृ.सं.105, गीताप्रेस गोरखपुर
12 https://sites.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/quantum_theory_waves/index.html
13 अपरोक्षानुभूति (203), श्लो.49, पृ.सं.13, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत्
14 विवेक-चूडामणि श्लो.230, पृ.सं.63, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
15 विवेक-चूडामणि श्लो.220, पृ.सं.61, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
16 विवेक-चूडामणि श्लो.233, पृ.सं.64, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_relativity
18 विवेक-चूडामणि श्लो.124, पृ.सं.36, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
19 आत्मबोध श्लो.14, पृ.सं.17, श्यामकाशी प्रेस, मथुरा
20 विवेक-चूडामणि श्लो.131, पृ.सं.37, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
21 विवेक-चूडामणि श्लो.232, पृ.सं.64, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071
22 विवेक-चूडामणि श्लो.47, पृ.सं.16, गीताप्रेस गोरखपुर, संवत् 2071


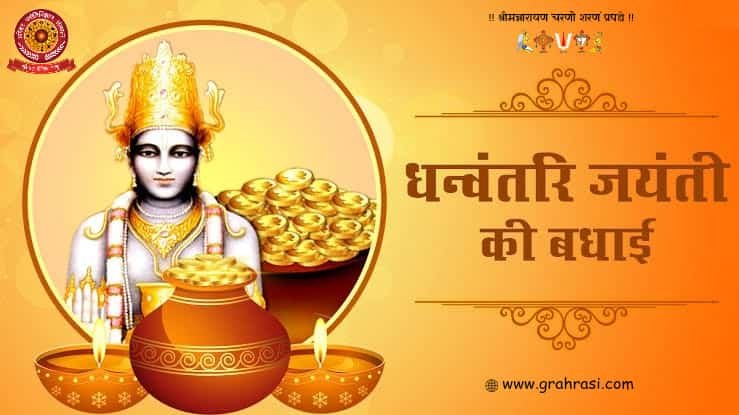
बहुत शानदार प्रस्तुती थी ।
आपके द्वारा जो व्याख्यान किया गया है बहुत उपयोगी है
जनमानस के कल्याण के लिए ।
हरि ओम नारायण
यह एक पहला आर्टिकल है, जिसने शंकराचार्य के कार्य को इतनी गहराई से समझा और वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनो दृष्टिकोण को आम जनमानस के सामने रखा है।।।
मैं ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।